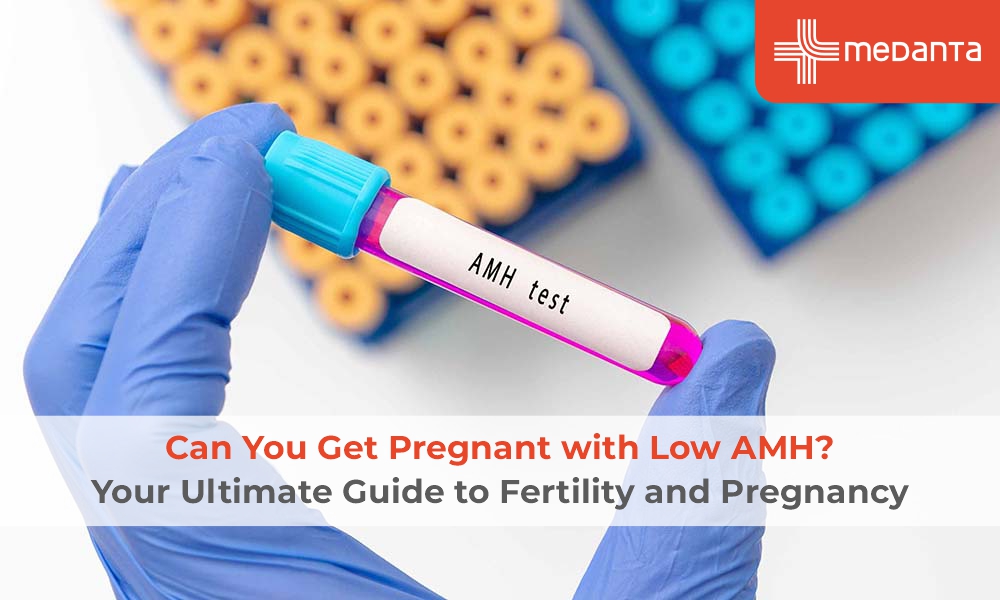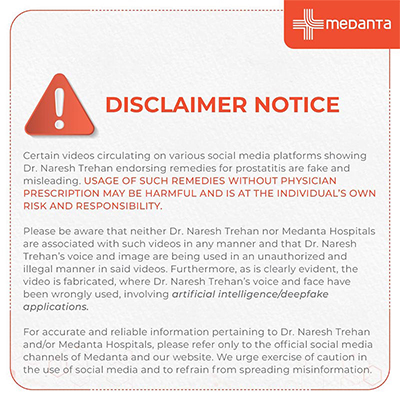पार्किसंस की नैदानिक विशेषताओं के आधार पर उसका निदान

पार्किंसंस रोग सबसे ज्यादा 60 साल की बाद की उम्र के लोगों होता है. इस दौरान शरीर का सबसे काम करने वाला हिस्सा प्रभावित होता है. हालांकि यह भी माना जाता है कि, पार्किंसंस रोग किसी आनुवांशिक स्थिति के कारण भी हो सकता है. इसे कंट्रोल तो किया जा सकता है लेकिन, इसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता. एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसे कई उपचार हैं, जो इसके लक्षणों को दूर करने में मददगार साबित होते हैं. इस बीमारी के होने पर मांसपेशियों में कठोरता, बोलचाल में बदलाव और चलने फिरने तक में बदलाव महसूस होने लगता है.
50 से 60 साल के बीच में शुरू होने वाला पार्किंसंस रोग के बारे में ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं होती. इस बीमारी का इलाज कोर्स के तौर पर किया जाता है. लेकिन यह बीमारी ज्यादा पुरानी हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं होता. अगर पार्किंसंस रोग को एक प्रगतिशील तंत्रिका से सम्बंधी विकार कहेंगे तो गलत नहीं होगा. इससे जुड़ी कुछ ऐसी समीक्षा है जो उन विशेषताओं पर जोर देने के साथ पार्किंसंस रोग की नैदानिक विशेषताओं का वर्णन करती है जो इसे अन्य पार्किन्सोनियन के विकारों से अलग करती है.
पार्किंसंस रोग की नैदानिक विशेषताओं का आंकलन करने वाले अध्ययनों की पहचान करने के लिए एक तरह की मेडलाइन की खोज की गयी थी. जिसमें पार्किंसंस रोग, उसके निदान, संकेत और लक्षण शामिल थे.
हालांकि पार्किंसंस रोग के निदान के लिए कोई निश्चित परीक्षण नहीं है. नैदानिक मानदंडों के आधार पर बात करें तो इसका रोग का निदान किया जाना चाहिए. रेस्ट ट्रेमर, ब्रैडीकिनेसिया के साथ पोस्त्युरल रिफ्लेक्स में कमी पार्किंसंस रोग के लक्षण में शामिल हैं. वहीं अन्य नैदानिक विशेषताओं में मोटर लक्षण भी शामिल हैं. जिसमें हाइपोमिमिया, डिसरथ्रीया, सियालोरिय जैसे लक्षण शामिल हैं. गैर मोटर लक्षणों में ऑटोनोमिक डिसफंक्शन और नींद से सम्बंधित परेशानियां घेरने लगती हैं.
पार्किंसंस रोग का क्या है इतिहास?
साल 1817 में जेम्स पार्किंसन ने पहली बार क्लिनिकल सिंड्रोम के बारे में बताया. जो बिमारी बाद में उनके नाम पर हो गयी. शरीर के किसी हिस्से में कंपकंपी के कुल छह मामलों की उन्होंने पहचान की. जिनमें से तीन की उन्होने खुद व्यक्तिगत तरीके से जांच की. बाद में 19वीं शताब्दी में चारकोट ने इस बीमारी को मैलाडी डी पार्किंसंस यानि की पार्किंसंस रोग के रूप में पहचाना. इतना ही नहीं चारकोट ने पार्किंसंस रोग के बिना कंपकंपी के रूपों को भी पहचाना और इस बात को कहा कि, इस बीमारी में धीरे-धीरे कमजोरी और कमजोर मांसपेशियों का बढ़ना बताया. इस विवरण के करीब 100 साल से भी ज्यादा समय से पार्किंसंस को पहचाना जाने लगा. इसके अलावा 140 साल बीत जाने के बात डोपामाइन कार्लसन और उनके साथियों ने लंदन, स्वीडन में इसे न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में खोजा गया. उन्होंने बताया था कि, पार्किंसंस रोग के साथ रोगियों के स्ट्रेटम में डोपमाइन की मात्रा कम हो जाती है. जिसके बाद साल 2000 में कार्ल्ससन को मेडिकल में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
क्या हैं नैदानिक सुविधाएं?
पार्किंसंस रोग की ख़ास चार विशेषताएं हैं. जिन्हें टीआरएपी के नाम से जाना जा सकता है. जिसमें कंपन, कठोरता, अकिनेसिया ब्रैडीकिनेसिया और पोस्टुरल अस्थिरता शामिल है. इसके अलावा पार्किंसनिज़्म की अन्य विशेषताओं में फ्लेक्स्ड पोस्चर और फ्रीजिंग को भी शामिल किया गया है, जिसमें पार्किंसंस रोग सबसे समान्य है. पार्किंसंस रोग से प्रभावित लोगों की लाइफस्टाइल की वजह से इसके प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है.
रेटिंग पैमोनों का इस्तेमाल
पार्किंसंस बीमारी के रोगियों में मोटर की खराबी और विकलांगता के मूल्यांकन के लिए कई रेटिंग पैमानों का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन इनमें से ज्यादातर पैमानों की वैद्यता और विश्वसनीयता के लिए पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया जाता. इस तरह के पैमाने का इस्तेमाल आमतौर पर एक रोगी की दूसरे रोगी से तुलना करने के लिए किया जाता है. चरण दर चरण बात की जाए तो, इस बीमारी के संकेत पहचनाना मुश्किल होता है. पार्किंसंस रोग के संकेत और लक्षण हर किसी में अलग-अलग तरह के हो सकते हैं. ज्यादातर मामलों में किसी का ध्यान इसके लक्षणों की ओर नहीं जाता. इसके लक्षण अक्सर शरीर के एक तरफ से शुरू होते हैं और उस तरफ को बेहद कमजोर बना देते हैं. पार्किंसंस रोग रेटिंग स्केल यानि की यूपीडीआरएस के जरिये विकलांगता और हानि का आंकलन करने के लिए सबसे अच्छा पैमाना है.
पार्किंसंस रोग को ट्रैक करने के लिए यूपीडीआरएस का इस्तेमाल करने वाले अध्यनों की मानें तो पार्किंसंस रोग का कोई कोर्स नहीं है और ये कंट्रोल हो सकता है. शोध के मुताबिक जिन रोगियों की उम्र ज्यादा होती है शुरुआत में पार्किंसंस रोग पीआईजीडी के रूप में होता है. वहीं कम उम्र में पार्किंसंस रोग कंपकंपी से शुरू हो सकता है. वहीं दूसरी ओर कई अध्यनों से ये भी पता चलता है कि, पुराने रोगियों की तुलना में नये रोगियों में लेवोडोपा डिस्केनेसिया का ज्यादा खतरा होता है.
ब्रैडीकिनेसिया
पार्किंसंस रोग की सबसे विशिष्ट नैदानिक विशेषताओं में ब्रैडीकिनेसिया शामिल हैं. हालांकि इसे तनाव सहित अन्य विकारों में भी देखा जा सकता है. ब्रैडीकिनेसिया बेसल गैन्ग्लिया उन्हीं विकारों की पहचान है. ब्रैडीकिनेसिया में कई तरह के संकेत देखे जा सकते हैं, जिनमें लार आना, मोनोटोनिक और हाइपोफोनिक डिसरथ्रिया, चेहरे पर पीलापन बढ़ना, पलकें कम झपकना और चलते वक्त हाथ ना हिलना शामिल है. ब्रैडीकिनेसिया पार्किंसंस रोग के सबसे आसानी से पहचाने जाने वाले लक्षणों में से एक है. इसे किसी भी न्यूरोलॉजिकल टेस्ट से पहले ही पहचाना जा सकता है. ब्रैडीकिनेसिया जे आकलन में आमतौर पर रोगियों के हाथ की तेजी, उंगलियों के टैप, हैंड ग्रिप्स, हैंड प्रॉनेशन-सुपिनेशन और हील टैप करना शामिल होता है.
रेस्ट ट्रेमर पार्किंसंस रोग का सबसे आम और आसानी से पहचाने जाने वाला लक्षण है. एक तरफ झनझनाहट के साथ हार्टबीट भी प्रभावित होती है. ये अहसास अक्सर शरीर के बाहरी हिस्से में होता है. हाथ में झनझनाहट को सुपिनेशन प्रोनेशन के रूप में जाना जाता है. जो एक हाथ से दूसरे हाथ में फैलता है. पार्किंसंस रोग में रोगियों को होठ, ठुड्डी, जबड़ा और पैर में भी झनझनाहट महसूस हो सकती है.
पार्किंसंस रोग से जुड़ी नैदानिक विशेषताओं के आधार पर इसे पहचाना जा सकता है. लेकिन इसका उपचार करना सम्भव नहीं है. पार्किंसंस के असर को कम करने के लिए दवाओं का सेवन किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा लाइफस्टाइल में बदलाव करना भी बेहद जरूरी है.